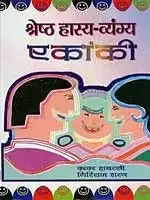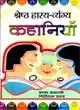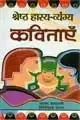|
नाटक-एकाँकी >> श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य एकांकी श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य एकांकीकाका हाथरसी व गिरिराज शरण
|
144 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हास्य-व्यंग्य : जीवन के अंग
जिस प्रकार विरोधी दल के नेताओं में नयी-नयी योजनाएं सूझती हैं। उसी तरह
ट्रेन में यात्रा करते समय हमारे मस्तिष्क में विचित्र कल्पनाएं उछल-कूद
मचाती हैं।
उस दिन डॉ० गिरिराजशरण के साथ यात्रा में स्टेशन पर मालूम हुआ कि गाड़ी एक घंटे लेट है। हमारे परिचित टी० टी० बाबू मिले तो हमने कहा, ‘‘क्या हो गया है, इमरजेंसी के बाद ? रोजाना गाड़ियां लेट आती हैं।’’ टी० टी० बाबू कवियों की संगत करते-करते काव्यरसिक बन गये थे। कहने लगे, ‘‘अजी काका, ट्रेन तो एक कुंआरी कन्या के समान है जो ‘मिस’ तो होती ही हैं, ‘लेट’ भी जाती हैं और ‘मेकअप’ भी करती है। अधिक मनचली हुई तो चलते-चलते सीटी बजाती है।’’ उनकी यह तुलनात्मक विवेचना सुनकर एक हास्यकवि ने तो इसपर कविता भी बना डाली थी।
गिरिराज जी ने कहा, ‘‘काका जी, आजकल हास्य-व्यंग्य के लेखक अच्छा लिख रहे हैं और आप स्वयं भी उनकी प्रशंसा करते हैं, क्यों न वर्तमान हास्य-व्यंग्याचार्यों की रचनाओं के संकलन तैयार किये जायें। प्रभात प्रकाशन इसे प्रकाशित करने को तैयार है। आपके पास तो बहुत-सा मैटर होगा। मैं जानता हूँ कि हास्य-व्यंग्य पर जो भी लेख या कविता आपको पसंद आती है, उसकी कटिंग आप एक फाइल में डाल लेते हैं।’’ ‘घर का भेदी लंका ढाये’ यह कहावत याद आयी और हमें स्वीकृतिसूचक सिर हिलाना ही पड़ा।
फिर वे बोले, ‘‘हास्य और व्यंग्य को कुछ साहित्यकार अलग-अलग मनाते हैं इस बारे में आपका विचार ? हमने कहा, ‘‘हास्य और व्यंग्य एक गाड़ी के दो पहिये हैं। हास्य के बिना व्यंग्य में मजा नहीं आता और व्यंग्य के बिना हास्य में स्वाद नहीं आता। दोनों बराबर एक-दूसरे का साथ दें तभी जन-गण-मन की मनोरंजनी गाड़ी ठीक से चलती है। अकेला व्यंग्य निंदा का रूप ले लेता है और अकेला हास्य भड़ैती का सूचक बन जाता है।’’ व्यंग्य का अंग और भी स्पष्ट करते हुए हमने कहा, ‘‘जिसपर व्यंग्य-बाण छोड़ा जाये वह तिलमिलाकर कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाये तो समझिये व्यंग्यकार सफल हुए।
इसके विरुद्ध वह व्यक्ति अपनी बेइज्जती समझकर व्यंग्यकार पर आक्रमण करने को तैयार हो जाये अथवा बदले में गाली देने लगे मैं उस व्यंग्य को व्यंग्य न मानकर अपमान या निंदा की संज्ञा ही दूँगा।’’
आप कड़ी से कड़ी बात कह जाइये, उसमें जरा-सा हास्य का पुट दीजिये। फिर देखिये उसका प्रभाव। पिछले दिनों मेरठ में कवि सम्मेलन हुआ। वे जिस समय मंच पर आये उस समय प्रसिद्ध गीतकार नीरज गीत सुना रहे थे। नीरज जी का गीत समाप्त हुआ और आवाज लगी कि काका हाथरसी आयें ? मैंने कहा, ‘‘श्रीमान जी के आने से पूर्व मैं कई कविताएँ सुना चुका हूँ और अभी कई शेष हैं, उन्हें सुनवाइए।’’ उत्तर मिला, ‘‘नहीं आप ही आइये।’’ मैंने श्री राजनारायण को लक्ष्य करते हुए कहा, ‘‘श्रीमान मैंने तो आज ही आपके सम्मान में छह पंक्तियां लिखी हैं। नाराज न हों तो सुना दूँ।’’ मैंने सुनायाः
उस दिन डॉ० गिरिराजशरण के साथ यात्रा में स्टेशन पर मालूम हुआ कि गाड़ी एक घंटे लेट है। हमारे परिचित टी० टी० बाबू मिले तो हमने कहा, ‘‘क्या हो गया है, इमरजेंसी के बाद ? रोजाना गाड़ियां लेट आती हैं।’’ टी० टी० बाबू कवियों की संगत करते-करते काव्यरसिक बन गये थे। कहने लगे, ‘‘अजी काका, ट्रेन तो एक कुंआरी कन्या के समान है जो ‘मिस’ तो होती ही हैं, ‘लेट’ भी जाती हैं और ‘मेकअप’ भी करती है। अधिक मनचली हुई तो चलते-चलते सीटी बजाती है।’’ उनकी यह तुलनात्मक विवेचना सुनकर एक हास्यकवि ने तो इसपर कविता भी बना डाली थी।
गिरिराज जी ने कहा, ‘‘काका जी, आजकल हास्य-व्यंग्य के लेखक अच्छा लिख रहे हैं और आप स्वयं भी उनकी प्रशंसा करते हैं, क्यों न वर्तमान हास्य-व्यंग्याचार्यों की रचनाओं के संकलन तैयार किये जायें। प्रभात प्रकाशन इसे प्रकाशित करने को तैयार है। आपके पास तो बहुत-सा मैटर होगा। मैं जानता हूँ कि हास्य-व्यंग्य पर जो भी लेख या कविता आपको पसंद आती है, उसकी कटिंग आप एक फाइल में डाल लेते हैं।’’ ‘घर का भेदी लंका ढाये’ यह कहावत याद आयी और हमें स्वीकृतिसूचक सिर हिलाना ही पड़ा।
फिर वे बोले, ‘‘हास्य और व्यंग्य को कुछ साहित्यकार अलग-अलग मनाते हैं इस बारे में आपका विचार ? हमने कहा, ‘‘हास्य और व्यंग्य एक गाड़ी के दो पहिये हैं। हास्य के बिना व्यंग्य में मजा नहीं आता और व्यंग्य के बिना हास्य में स्वाद नहीं आता। दोनों बराबर एक-दूसरे का साथ दें तभी जन-गण-मन की मनोरंजनी गाड़ी ठीक से चलती है। अकेला व्यंग्य निंदा का रूप ले लेता है और अकेला हास्य भड़ैती का सूचक बन जाता है।’’ व्यंग्य का अंग और भी स्पष्ट करते हुए हमने कहा, ‘‘जिसपर व्यंग्य-बाण छोड़ा जाये वह तिलमिलाकर कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाये तो समझिये व्यंग्यकार सफल हुए।
इसके विरुद्ध वह व्यक्ति अपनी बेइज्जती समझकर व्यंग्यकार पर आक्रमण करने को तैयार हो जाये अथवा बदले में गाली देने लगे मैं उस व्यंग्य को व्यंग्य न मानकर अपमान या निंदा की संज्ञा ही दूँगा।’’
आप कड़ी से कड़ी बात कह जाइये, उसमें जरा-सा हास्य का पुट दीजिये। फिर देखिये उसका प्रभाव। पिछले दिनों मेरठ में कवि सम्मेलन हुआ। वे जिस समय मंच पर आये उस समय प्रसिद्ध गीतकार नीरज गीत सुना रहे थे। नीरज जी का गीत समाप्त हुआ और आवाज लगी कि काका हाथरसी आयें ? मैंने कहा, ‘‘श्रीमान जी के आने से पूर्व मैं कई कविताएँ सुना चुका हूँ और अभी कई शेष हैं, उन्हें सुनवाइए।’’ उत्तर मिला, ‘‘नहीं आप ही आइये।’’ मैंने श्री राजनारायण को लक्ष्य करते हुए कहा, ‘‘श्रीमान मैंने तो आज ही आपके सम्मान में छह पंक्तियां लिखी हैं। नाराज न हों तो सुना दूँ।’’ मैंने सुनायाः
नाटक में ज्यों विदूषक, जोकर सरकस माहिं,
कवि सम्मेलन का मजा बिना हास्यकवि नाहिं।
बिना हास्यकवि नाहिं, हास्य का भारी पल्ला,
अकबर के दरबार बीरबल का था हल्ला।
यह उदाहरण देते हैं काका इस कारण,
आवश्यक हैं संसद में श्री राजनारायण।
कवि सम्मेलन का मजा बिना हास्यकवि नाहिं।
बिना हास्यकवि नाहिं, हास्य का भारी पल्ला,
अकबर के दरबार बीरबल का था हल्ला।
यह उदाहरण देते हैं काका इस कारण,
आवश्यक हैं संसद में श्री राजनारायण।
मंत्री जी ने एकदम उछलकर हमसे हाथ मिलाया। तब मैंने अनुभव किया कि व्यंग्य
का प्रयोग ढंग से किया जाए तो उसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है।
एक उदाहरण और देखिये। हमारी मिसरानी प्रायः मैली धोती पहनकर आया करती थी। मैंने उसे कई बार टोका, लेकिन वह टाल देती। एक दिन मैंने व्यंग्य की बंदूक छोड़ दी और कहा, ‘‘मिसरानी जी, यह धोती जो तुम पहनकर आती हो, क्यों इसका सत्यनाश करती हो, देवछट का मेला रहा है, उसके लिए रख लो न इसे।’’ वह धोती का पल्ला मुँह पर रखकर इतना हँसी कि चूल्हे की रोटी जल गयी। दूसरे ही दिन स्वच्छ वस्त्रों में आना प्रारम्भ कर दिया।
यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग व्यंग्य के टीले पर बैठकर अपने को महान व्यंग्यकार समझते हैं और जिस व्यंग्य में सरल हास्य भी रहता है, उसे निम्नकोटि का समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ‘‘हम स्वयं को जो समझते हैं, अपने बारे में जो जानते हैं, जरूरी नहीं है, वह सही हो, व्यक्ति तो व्यक्ति, पूरा युग भी अपनी असलियत नहीं पहचान पाता।’’
वस्तुतः व्यंग्य में यदि हास्य नहीं होगा तो वह कोतवाल का हंटर हो जाएगा। उसकी पीड़ा से तिलमिलाकर अभियुक्त कैसा अनुभव करेगा, उसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस कार्य के लिए न्यायालय पहले से ही मौजूद है, फिर व्यंग्य की क्या जरूरत है। हास्य-मिश्रित व्यंग्य सीधा प्रहार करता है और आपको चोट भी नहीं लगती। लगती भी है तो वह चोट आपके हृदय-परिवर्तन में सहायक होती है। स्व० हृषीकेश चतुर्वेदी कहा करते थे कि ‘‘मजाक करना नहीं है, मजाक करो तो तमीज के साथ करो, वरना चुप रहो।’’
हास्य-व्यंग्य की रचनात्मक धारा से ये पुस्तकें आपके सामने हैं, जिसमें हास्य-व्यंग्य की श्रेष्ठ कविताओं, कहानियों, निबन्धों और एकांकियों को अलग-अलग संकलित किया गया है। इनके रचनाकारों ने रचनाएं भेजने में जो तत्परता दिखायी है इनके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार हमारी उस यात्रा में एक ऐसा काम हो गया जिससे हजारों हास्य-व्यंग्य-प्रेमियों को शिक्षात्मक मनोरंजन प्राप्त होगा और वे ‘हास्य-व्यंग्य जीवन के अंग’ इस सूत्र को स्वीकार करेंगे।
एक उदाहरण और देखिये। हमारी मिसरानी प्रायः मैली धोती पहनकर आया करती थी। मैंने उसे कई बार टोका, लेकिन वह टाल देती। एक दिन मैंने व्यंग्य की बंदूक छोड़ दी और कहा, ‘‘मिसरानी जी, यह धोती जो तुम पहनकर आती हो, क्यों इसका सत्यनाश करती हो, देवछट का मेला रहा है, उसके लिए रख लो न इसे।’’ वह धोती का पल्ला मुँह पर रखकर इतना हँसी कि चूल्हे की रोटी जल गयी। दूसरे ही दिन स्वच्छ वस्त्रों में आना प्रारम्भ कर दिया।
यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग व्यंग्य के टीले पर बैठकर अपने को महान व्यंग्यकार समझते हैं और जिस व्यंग्य में सरल हास्य भी रहता है, उसे निम्नकोटि का समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ‘‘हम स्वयं को जो समझते हैं, अपने बारे में जो जानते हैं, जरूरी नहीं है, वह सही हो, व्यक्ति तो व्यक्ति, पूरा युग भी अपनी असलियत नहीं पहचान पाता।’’
वस्तुतः व्यंग्य में यदि हास्य नहीं होगा तो वह कोतवाल का हंटर हो जाएगा। उसकी पीड़ा से तिलमिलाकर अभियुक्त कैसा अनुभव करेगा, उसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस कार्य के लिए न्यायालय पहले से ही मौजूद है, फिर व्यंग्य की क्या जरूरत है। हास्य-मिश्रित व्यंग्य सीधा प्रहार करता है और आपको चोट भी नहीं लगती। लगती भी है तो वह चोट आपके हृदय-परिवर्तन में सहायक होती है। स्व० हृषीकेश चतुर्वेदी कहा करते थे कि ‘‘मजाक करना नहीं है, मजाक करो तो तमीज के साथ करो, वरना चुप रहो।’’
हास्य-व्यंग्य की रचनात्मक धारा से ये पुस्तकें आपके सामने हैं, जिसमें हास्य-व्यंग्य की श्रेष्ठ कविताओं, कहानियों, निबन्धों और एकांकियों को अलग-अलग संकलित किया गया है। इनके रचनाकारों ने रचनाएं भेजने में जो तत्परता दिखायी है इनके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार हमारी उस यात्रा में एक ऐसा काम हो गया जिससे हजारों हास्य-व्यंग्य-प्रेमियों को शिक्षात्मक मनोरंजन प्राप्त होगा और वे ‘हास्य-व्यंग्य जीवन के अंग’ इस सूत्र को स्वीकार करेंगे।
-काका हाथरसी
जैसा मैं सोचता हूँ
यह सौभाग्य की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से हास्य और
व्यंग्यपरक
विधा पर विचार होने लगा है। जिस शिल्प को महत्त्व नहीं दिया जाता था, जिस
कथ्य को यों ही उड़ा दिया जाता था, समीक्षक नाक-भौं सिकोड़ते थे, आलोचक
कन्नी काट जाते थे, अब कम–से-कम इतना तो हुआ समीक्षकों ने उसपर
बातचीत चलायी है।
पर दुर्भाग्य है कि यह बातचीत अभी तक सुलझे हुए वस्तुगत निष्कर्षों तक नहीं पहुँची। हमारे देश के जाने-माने हिंदी व्यंग्यकार भी जब सृजनात्मक लेखन से हटकर व्यंग्य की प्रतिभा पर बात करते हैं तो उसे एक अजीब-सी स्वायत्तता प्रदान करना चाहते हैं। मसलन व्यंग्य है, वह ऊंचे दर्जे की चीज है, हास्य से उसका कोई लेना-देना नहीं, हास्य बेहद घटिया चीज है। न केवल हास्य-व्यंग्य के अंतः सम्बन्धों को समझने में गड़बड़ी है, बल्कि हास्य और व्यंग्य के मूल उत्सों की पहचान भी इस गड़बड़ी में खो जाती है।
हमें यहां बस दो बातें करनी हैं। पहली, हास्य और व्यंग्य की रचना-प्रक्रिया और दूसरी, हास्य और व्यंग्य के आपसी रिश्तों के संबंधों में। ज्ञान और संवेदना का अविच्छिन्न संबंध है। विशेषकर इस शताब्दी में अगर कोई ज्ञान रहित संवेदना की बात करता है या संवेदना-रहित ज्ञान की चर्चा करता है तो त्रुटि पर है। हास्य को हम संवेदना का एक प्रकार मान सकते हैं। व्यंग्य में विचार या ज्ञान की प्रधानता स्वीकारी ही जाती है। मुक्तिबोध द्वारा गढ़े गये परिभाषित शब्द-युग्मों-ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान-के वजन पर हमारा मन भी ऐसे शब्दयुग्म बनाने को करता है। यात्रा और अनुपात के आधार पर हमें हास्य को ‘हास्यात्मक व्यंग्य’ और व्यंग्य को ‘व्यंग्यात्मक हास्य’ कहना चाहिए। ‘तर’ और ‘तम’ का अंतर भी से स्पष्ट प्रकट हो जायेगा और व्यंग्य को व्यंग्य एवं हास्य में द्वैत-पैदा करनेवालों को जवाब भी मिल जायेगा।
हास्य और व्यंग्य के उत्स पर विचार करते हुए व्यंग्यचित्रकार आबू की एक बड़ी मजेदार बाद आती है। उन्होंने बड़े मासूम अंदाज में कहीं लिखा हैः जरा सोचिए कि जानवर क्यों नहीं हँसते। सीधा-सा उत्तर है, उनके पास किसी पर हंसने का कारण नहीं होता हैं, क्योंकि वे सब समान हैं। असमान होते तो एक-दूसरे पर हंसते, व्यंग्य करते।’’
कहने को बात में लॉजिक नहीं है लेकिन काफी हद तक बात साफ हो जाती है। असमानता हास्य और व्यंग्य का कारण है। हम अपने बराबर वालों पर नहीं हँसते, हँसते हैं तो छोटों पर या बड़ों पर। हँसते हैं छोटों पर तो बड़े साथ देते हैं। बड़ों पर हँसते हैं तो छोटे साथ देते हैं। बड़ों की संख्या कम, छोटों की ज्यादा है इसलिए अधिकांशः छोटे ही बड़ों पर हँसकर उदात्तीकरण करते हैं। केले के छिलके पर कोई गरीब फटेहाल फिसल जाए तो शायद हँसी न आए; हो सकता है कि कोई सहृदय सज्जन उसे उठाने बढ़े लेकिन यदि मोटे लाला जी उससे फिसल जायें तो उठाने की बात तो दूर कुछ लोग खिलखिलाकर कुछ नजरें बचाकर, तो कुछ खुलेआम हंसेगे और काफी देर तक हँसते रहेंगे। देखा जाये तो इसमें हँसने की कोई बात नहीं है। इसमें बेचारे लाला जी का क्या दोष कि वे फिसल गये किंतु बारीकी से देखा जाये तो हँसने की बात निकलती है। थुल-थुल लाला जी के फिसलने में एक सहायिका उनकी तोंद भी थी, जिसके साथ दूसरों को चूसने का अच्छा-खासा अतीत जुड़ा हुआ है। असमानता का यह अहसास हमें यह तो याद दिलाता ही है कि हमें उन जैसी नहीं, लेकिन एक ही झटके में उसे तिरोहित कर उदात्तीकृत कर देता है। तोंद से संबद्ध शोषण की अतीत गाथा हमारी विचार-प्रक्रिया से टकराती है और हास्य में अंतर्निहित व्यंग्य धीरे-धीरे उभरने लगता है। इसे हम हास्यात्मक व्यंग्य कहेंगे।
यदि कोई व्यंग्यकार इस घटना में अपनी कल्पना विचार-भावना और बुद्धि का योग देकर इस चित्र को कुछ इस तरह खींच के मोटे मंत्री जी हाथ में फाइलें दबाये कैबिनेट की मीटिंग अटैंड करने की फुर्ती में हैं कि फिसल गये। खादी के कुरते के नीचे मिल के रेशम की बनियान झांकने लगी, फाइलों में से फिल्मी पत्रिका गिर पड़ी, कुरते की जेब से विदेशी पेन सरक गया, एक तरफ बत्तीसी जा गिरी-हँसी तो इस चित्र को पढ़-देखकर भी आयेगी किंतु हम इसे व्यंगात्मक हास्य कहेंगे।
हास्य-व्यंग्य के उत्स और उनके संबंधों की बात साथ-साथ चल रही है। उत्स के बारे में एक बात और कह देंगे जो प्रकारांतर से पिछली बात का विस्तार ही है। युग बदलता है परिस्थितियां बदलती हैं, परिवेश बदलता है किंतु कुछ क्षेत्रों में परंपराएं और रूढियां नहीं बदल पातीं। पुरानी मूल्य-व्यवस्था से जकड़न नहीं टूट पाती। नये परिवेश में वे अपनी उपयोगिता खो चुकती हैं। अतः विद्रूपित हो जाती हैं। यह विद्रूप भी हास्य-व्यंग्य का जन्मदाता होता है, क्योंकि इसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां, विडंबनाएँ और सामाजिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं।
परक विडंबनाएं जितनी अधिक होंगी, उतनी ही वहाँ हास्य और व्यंग्य की संभावनाएं होंगी।
विसंगितयों और विडंबना-विकारों के रहते कोई भी व्यंग्य हास्य-शून्य नहीं हो सकता और कोई भी हास्य व्यंग्य के बिना अस्तित्व नहीं रख सकता। हास्य से हमारा अभिप्राय मसखरेपन, मजाक या जोकरी से नहीं है, हास्य से हमारा तात्पर्य है—हास्यात्मक व्यंग्य।
सामान्य समीक्षकों को हास्य-व्यंग्य के अंतःसंबंधों पर पुनर्विचार करने की अदना राय के साथ हास्य-व्यंग्य के संकलन सामने हैं। इन्हें कहीं भी आप हंसने से वंचित नहीं होंगे, साथ ही व्यंग्य की मार से भी बच पाएंगे।
पर दुर्भाग्य है कि यह बातचीत अभी तक सुलझे हुए वस्तुगत निष्कर्षों तक नहीं पहुँची। हमारे देश के जाने-माने हिंदी व्यंग्यकार भी जब सृजनात्मक लेखन से हटकर व्यंग्य की प्रतिभा पर बात करते हैं तो उसे एक अजीब-सी स्वायत्तता प्रदान करना चाहते हैं। मसलन व्यंग्य है, वह ऊंचे दर्जे की चीज है, हास्य से उसका कोई लेना-देना नहीं, हास्य बेहद घटिया चीज है। न केवल हास्य-व्यंग्य के अंतः सम्बन्धों को समझने में गड़बड़ी है, बल्कि हास्य और व्यंग्य के मूल उत्सों की पहचान भी इस गड़बड़ी में खो जाती है।
हमें यहां बस दो बातें करनी हैं। पहली, हास्य और व्यंग्य की रचना-प्रक्रिया और दूसरी, हास्य और व्यंग्य के आपसी रिश्तों के संबंधों में। ज्ञान और संवेदना का अविच्छिन्न संबंध है। विशेषकर इस शताब्दी में अगर कोई ज्ञान रहित संवेदना की बात करता है या संवेदना-रहित ज्ञान की चर्चा करता है तो त्रुटि पर है। हास्य को हम संवेदना का एक प्रकार मान सकते हैं। व्यंग्य में विचार या ज्ञान की प्रधानता स्वीकारी ही जाती है। मुक्तिबोध द्वारा गढ़े गये परिभाषित शब्द-युग्मों-ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान-के वजन पर हमारा मन भी ऐसे शब्दयुग्म बनाने को करता है। यात्रा और अनुपात के आधार पर हमें हास्य को ‘हास्यात्मक व्यंग्य’ और व्यंग्य को ‘व्यंग्यात्मक हास्य’ कहना चाहिए। ‘तर’ और ‘तम’ का अंतर भी से स्पष्ट प्रकट हो जायेगा और व्यंग्य को व्यंग्य एवं हास्य में द्वैत-पैदा करनेवालों को जवाब भी मिल जायेगा।
हास्य और व्यंग्य के उत्स पर विचार करते हुए व्यंग्यचित्रकार आबू की एक बड़ी मजेदार बाद आती है। उन्होंने बड़े मासूम अंदाज में कहीं लिखा हैः जरा सोचिए कि जानवर क्यों नहीं हँसते। सीधा-सा उत्तर है, उनके पास किसी पर हंसने का कारण नहीं होता हैं, क्योंकि वे सब समान हैं। असमान होते तो एक-दूसरे पर हंसते, व्यंग्य करते।’’
कहने को बात में लॉजिक नहीं है लेकिन काफी हद तक बात साफ हो जाती है। असमानता हास्य और व्यंग्य का कारण है। हम अपने बराबर वालों पर नहीं हँसते, हँसते हैं तो छोटों पर या बड़ों पर। हँसते हैं छोटों पर तो बड़े साथ देते हैं। बड़ों पर हँसते हैं तो छोटे साथ देते हैं। बड़ों की संख्या कम, छोटों की ज्यादा है इसलिए अधिकांशः छोटे ही बड़ों पर हँसकर उदात्तीकरण करते हैं। केले के छिलके पर कोई गरीब फटेहाल फिसल जाए तो शायद हँसी न आए; हो सकता है कि कोई सहृदय सज्जन उसे उठाने बढ़े लेकिन यदि मोटे लाला जी उससे फिसल जायें तो उठाने की बात तो दूर कुछ लोग खिलखिलाकर कुछ नजरें बचाकर, तो कुछ खुलेआम हंसेगे और काफी देर तक हँसते रहेंगे। देखा जाये तो इसमें हँसने की कोई बात नहीं है। इसमें बेचारे लाला जी का क्या दोष कि वे फिसल गये किंतु बारीकी से देखा जाये तो हँसने की बात निकलती है। थुल-थुल लाला जी के फिसलने में एक सहायिका उनकी तोंद भी थी, जिसके साथ दूसरों को चूसने का अच्छा-खासा अतीत जुड़ा हुआ है। असमानता का यह अहसास हमें यह तो याद दिलाता ही है कि हमें उन जैसी नहीं, लेकिन एक ही झटके में उसे तिरोहित कर उदात्तीकृत कर देता है। तोंद से संबद्ध शोषण की अतीत गाथा हमारी विचार-प्रक्रिया से टकराती है और हास्य में अंतर्निहित व्यंग्य धीरे-धीरे उभरने लगता है। इसे हम हास्यात्मक व्यंग्य कहेंगे।
यदि कोई व्यंग्यकार इस घटना में अपनी कल्पना विचार-भावना और बुद्धि का योग देकर इस चित्र को कुछ इस तरह खींच के मोटे मंत्री जी हाथ में फाइलें दबाये कैबिनेट की मीटिंग अटैंड करने की फुर्ती में हैं कि फिसल गये। खादी के कुरते के नीचे मिल के रेशम की बनियान झांकने लगी, फाइलों में से फिल्मी पत्रिका गिर पड़ी, कुरते की जेब से विदेशी पेन सरक गया, एक तरफ बत्तीसी जा गिरी-हँसी तो इस चित्र को पढ़-देखकर भी आयेगी किंतु हम इसे व्यंगात्मक हास्य कहेंगे।
हास्य-व्यंग्य के उत्स और उनके संबंधों की बात साथ-साथ चल रही है। उत्स के बारे में एक बात और कह देंगे जो प्रकारांतर से पिछली बात का विस्तार ही है। युग बदलता है परिस्थितियां बदलती हैं, परिवेश बदलता है किंतु कुछ क्षेत्रों में परंपराएं और रूढियां नहीं बदल पातीं। पुरानी मूल्य-व्यवस्था से जकड़न नहीं टूट पाती। नये परिवेश में वे अपनी उपयोगिता खो चुकती हैं। अतः विद्रूपित हो जाती हैं। यह विद्रूप भी हास्य-व्यंग्य का जन्मदाता होता है, क्योंकि इसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां, विडंबनाएँ और सामाजिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं।
परक विडंबनाएं जितनी अधिक होंगी, उतनी ही वहाँ हास्य और व्यंग्य की संभावनाएं होंगी।
विसंगितयों और विडंबना-विकारों के रहते कोई भी व्यंग्य हास्य-शून्य नहीं हो सकता और कोई भी हास्य व्यंग्य के बिना अस्तित्व नहीं रख सकता। हास्य से हमारा अभिप्राय मसखरेपन, मजाक या जोकरी से नहीं है, हास्य से हमारा तात्पर्य है—हास्यात्मक व्यंग्य।
सामान्य समीक्षकों को हास्य-व्यंग्य के अंतःसंबंधों पर पुनर्विचार करने की अदना राय के साथ हास्य-व्यंग्य के संकलन सामने हैं। इन्हें कहीं भी आप हंसने से वंचित नहीं होंगे, साथ ही व्यंग्य की मार से भी बच पाएंगे।
(डा.) गिरिराजशरण अग्रवाल
चमत्कार
उपेन्द्रनाथ अश्क
पात्र
-------------------------------------------------------
तुर्की टोपीवाला
लंबी चोटीवाला
कृपाणवाला
घंटीवाला
सफेद दाढ़ीवाला
अन्य राह-चलते लोग
-------------------------------------------------------
तुर्की टोपीवाला
लंबी चोटीवाला
कृपाणवाला
घंटीवाला
सफेद दाढ़ीवाला
अन्य राह-चलते लोग
-------------------------------------------------------
स्थान : एक बड़े नगर का एक बड़ा बाजार
समय : दिन
(रंगमंच के बायें कोने में ‘बाइबिल सोसायटी’ का महराबदार दरवाजा है। महराब के ऊपर बड़े-बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा है :
‘‘यीसू मसीह ने कहा, ‘उठ ! और कुमारी उठ बैठी !’’ यह बाइबिल सोसायटी एक बड़े खुले बाजार में है। रंगमंच के दायें कोने में बाइबिल सोसायटी के साथ की दुकान का आधा बोर्ड (जिस पर उप्पल एंड कंपनी लिखा हुआ है) और दरवाजे का आधा भाग साफ दिखाई देता है। बाइबिल सोसायटी और उप्पल एंड कंपनी की सीमाएं स्टेज के मध्य आकर मिलती हैं। बाइबिल सोसायटी की बिल्डिंग का रंग लाल है और दूसरी दुकान का मोतिया। दोनों दुकानों के आगे फुटपाथ है, जिस पर बिजली का एक खंभा भी उप्पल एंड कम्पनी के सामने दिखाई देता है। फुटपाथ के इस ओर बायें से दायें अथवा दायें से बायें को जानेवाली तारकोल की सड़क है।
पर्दा उठने पर बाजार साधारण रूप से चलता दिखाई देता है। लोग अपने मध्य में मग्न उधर से इधर और इधर से उधर आ-जा रहे हैं। एक फैसनेबुल लेडी उप्पल एंड कंपनी के दरवाजे में प्रवेश करती है। एक डाकिया बाइबिल सोसायटी के दरवाजे में से बाहर आता है।
कुछ क्षणों बाद बायी ओर से एक दुबला-पतला व्यक्ति सिर पर तुर्की टोपी रखे, गले में खुले गले की मैली-फटी कमीज और कमर में टखनों से ऊंचा, कदरे तंग, घुटनों पर (निरंतर पहने रहने के कारण) कुछ आगे को बढ़ा हुआ उटंग पायजामा पहने, सिगरेट के एक काली टीन के बक्से को रस्सी से खींचता हुआ प्रवेश करता है और दोनों दुकानों के मध्य आ खड़ा होता है।
पल-भर के लिए वह राह-चलते लोगों को देखता है, फिर ऊंचे स्वर में बाइबिल सोसाइयटी के दरवाजे पर लिखे हुए मॉटो (Motto) को पढ़ाता है।)
टोपीवाला : यीसू मसीह ने कहा, ‘‘उठ !’’ और कुमारी उठ बैठी। (सोसाटी के दरवाजे की ओर देखकर) बुलाओ अपने यीसू मसीह को कि वे मेरी मुर्दा मछली को जिंदा करे। (फिर दांत पीसते हुए, मुंह चिढ़ाकर और राग-चलतों को सुनाकर) यीसू मसीह ने कहा, ‘‘उठ !’’ और कुमारी उठ बैठी। (फिर दरवाजे की ओर देखकर) बुलाओ अपने उस मसीह को कि इस मुर्दा मछली को जिंदा करे।
(उसकी आवाज सुनकर तीन-चार राह-चलते इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें एक लंबी टोपीवाला भी है।)
टोपीवाला : (पूर्ववत् राह-चलतों को सुनाकर) मसीह की सबसे बड़ी करामात यह थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। उन्होंने जेरस की मुर्दा बेटी को छुआ और वो उठ बैठी तो वो क्यों आकर मेरी इस मुर्दा मछली को नहीं जिलाते। (दरवाजे की ओर देखकर) निकालो अपने उस मसीह को कि मेरी इस मुर्दा मछली को जिंदा करे।
(कुछ और लोग आ जाते हैं, जिनमें एक कृपाणवाला भी है।)
चोटीवाला : (आगे बढ़कर) क्यों भाई क्या बात है ?
टोपीवाला : ‘अल मुबल्लिग’ में मैंने एक मारके का मजमून लिखा था, जिसमें ईसाई मजहब की बुनियादी खामियों पर दलील के साथ बहस की थी। मेरे इस लेख का कोई माकूल1 जवाब देने के बदले (सोसाटी के दरवाजे की ओर देखकर) पादरी बधावा-राम ने अपने अखबार के रसूले-पाक की करामातों पर एतराज किया है। मेराज2 की असलियत को समझना पादरी बधावाराम के बस की बात नहीं। कौन नहीं जानता कि खुदाबन्दे करीम ने अपने रसूल को सातों आसमानों की सैर करायी और वो भी इतने कम अर्से में कि जिस दरवाजे से रसूल-पाक गये थे, उसकी कुण्डी उनके वापस आने पर अभी हिल रही थी। इस मोजजे3 के कई मतलब निकल सकते हैं, लेकिन उन पर गौर करने के बजाय पादरी बधवाराम ने ओछे और लगव4 एतराज किये हैं।
कृपाणवाला : पर मियां, इस टीन के डिब्बे में क्या है ?
टोपीवाला : मछली।
कृपाणवाला : मछली !
टोपीवाला : हां, मुर्दा मछली ! मैं पादरी बधावाराम को चैलेंज देने आया हूं कि अगर सचमूच यीसू मसीह में यह ताकत थी कि वे मुर्दों को जिंदा कर देते थे और अगर सचमुच वो खुदा के बेटे थे, तो पादरी वधावाराम अपने उस खुदा के बेटे को बुलाये कि वो आकर मेरी इस मुर्दा मछली को जिलाये और अपनी मसीहाई का सुबूत दे।
चोटीवाला : पादरी बधावाराम ! (चोटी पर हाथ फेर और हंसते हुए अपने पास खड़े एक-दूसरे लंबी चोटीवाले साथी से) अरे ! यह वही बधावाराम है, जिसे हमने शुद्ध किया था परंतु जो हमारे कठिन सिद्धांत पर पूरा न उतर सका था।
(पादरी बधावाराम सोसायटी के दरवाजे से झांकते हैं।)
: (पादरी की ओर देखकर) हां पादरी साहब, बुलाइये अपने खुदा के बेटे को कि वह अपना चमत्कार दिखाकर इस मरी हुई मछली को पुनः जीवित करे (लोगों को सुनाकर) यदि भगवान अमर और सर्वव्यापक हैं तो भगवान का पुत्र अमर और सर्वव्यापक क्यों न होगा और क्यों न यहां आकर इस मुर्दा मछली को जीवित करेगा।
(कुछ लोग भीड़ में आकर सम्मिलित हो जाते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध चुपचाप भीड़ के एक ओर खड़ा तमाशा देखने लगता है।
एक हाथ में बैग उठाये और दूसरे में घंटी लिए एक व्यक्ति सबसे पीछे आकर खड़ा हो जाता है।)
----------------------------------------------------
1. माकूल-युक्तियुक्त। 2. मेंराज-पराकाष्ठा। 3. मोजजा-चमत्कार। 4. लगव-लचर।
टोपीवाला: (घंटी को देखकर नारा लगाता है।) आये खुदा का बेटा और मेरी इस मुर्दा मछली को जिंदा करे।
(पादरी बधावाराम फिर अंदर चले जाते हैं।)
चोटीवाला : (शिखा पर हाथ फेरते हुए) एक सभा में पादरी बधावाराम ने आर्यसमाजियों को मूस-पंथी कहा था—चूहे को शिवलिंग पर से प्रसाद उड़ाते देखकर महर्षि को जो दैवी प्रेरणा मिली थी, उसका उपहास उड़ाते हुए उनके व्यक्तित्व की निंदा की थी। (भाषण देने के अंदाज में हवा में हाथ घुमाते और एड़ियां उठाते हुए) महर्षि दयानंद पूर्ण ब्रह्मचारी थे, उनके मुख पर अद्भुत, अलौकिक तेज और उनके अंगों में अपार शक्ति थी। अपने योगबल से वे ऐसे आश्चर्यजनक बातें कर सकते थे, जो दूसरों को चमत्कार मालूम होती थीं। जालंधर में टिक्का साहब की गाड़ी को उन्होंने पीछे से पकड़ लिया। घोड़े शक्ति लगाकर थक गये। लेकिन वह तो ब्रह्मचारी का बल था, टस से मस न हुई गाड़ी। चमत्कार यह होता है। इसे बुद्धि स्वीकार करती है, परंतु....
कृपाणवाला : (जोश में आगे बढ़कर) इन्हीं पादरी साहब ने हमारे बाबा साहब बाबा गुरुनानक के चमत्कारों की भी आलोचना की थी और मोदीखाने की बात को लेकर मजाक उड़ाया था। वे तो सत्यावान1 पुरुष थे। ननकाना साहब के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। गुरु साहब के बहनोई जयगोपाल लोधी सुल्तान के यहां नौकर थे।
----------------------------------------------
1. सत्यावान—शक्तिशाली
समय : दिन
(रंगमंच के बायें कोने में ‘बाइबिल सोसायटी’ का महराबदार दरवाजा है। महराब के ऊपर बड़े-बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा है :
‘‘यीसू मसीह ने कहा, ‘उठ ! और कुमारी उठ बैठी !’’ यह बाइबिल सोसायटी एक बड़े खुले बाजार में है। रंगमंच के दायें कोने में बाइबिल सोसायटी के साथ की दुकान का आधा बोर्ड (जिस पर उप्पल एंड कंपनी लिखा हुआ है) और दरवाजे का आधा भाग साफ दिखाई देता है। बाइबिल सोसायटी और उप्पल एंड कंपनी की सीमाएं स्टेज के मध्य आकर मिलती हैं। बाइबिल सोसायटी की बिल्डिंग का रंग लाल है और दूसरी दुकान का मोतिया। दोनों दुकानों के आगे फुटपाथ है, जिस पर बिजली का एक खंभा भी उप्पल एंड कम्पनी के सामने दिखाई देता है। फुटपाथ के इस ओर बायें से दायें अथवा दायें से बायें को जानेवाली तारकोल की सड़क है।
पर्दा उठने पर बाजार साधारण रूप से चलता दिखाई देता है। लोग अपने मध्य में मग्न उधर से इधर और इधर से उधर आ-जा रहे हैं। एक फैसनेबुल लेडी उप्पल एंड कंपनी के दरवाजे में प्रवेश करती है। एक डाकिया बाइबिल सोसायटी के दरवाजे में से बाहर आता है।
कुछ क्षणों बाद बायी ओर से एक दुबला-पतला व्यक्ति सिर पर तुर्की टोपी रखे, गले में खुले गले की मैली-फटी कमीज और कमर में टखनों से ऊंचा, कदरे तंग, घुटनों पर (निरंतर पहने रहने के कारण) कुछ आगे को बढ़ा हुआ उटंग पायजामा पहने, सिगरेट के एक काली टीन के बक्से को रस्सी से खींचता हुआ प्रवेश करता है और दोनों दुकानों के मध्य आ खड़ा होता है।
पल-भर के लिए वह राह-चलते लोगों को देखता है, फिर ऊंचे स्वर में बाइबिल सोसाइयटी के दरवाजे पर लिखे हुए मॉटो (Motto) को पढ़ाता है।)
टोपीवाला : यीसू मसीह ने कहा, ‘‘उठ !’’ और कुमारी उठ बैठी। (सोसाटी के दरवाजे की ओर देखकर) बुलाओ अपने यीसू मसीह को कि वे मेरी मुर्दा मछली को जिंदा करे। (फिर दांत पीसते हुए, मुंह चिढ़ाकर और राग-चलतों को सुनाकर) यीसू मसीह ने कहा, ‘‘उठ !’’ और कुमारी उठ बैठी। (फिर दरवाजे की ओर देखकर) बुलाओ अपने उस मसीह को कि इस मुर्दा मछली को जिंदा करे।
(उसकी आवाज सुनकर तीन-चार राह-चलते इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें एक लंबी टोपीवाला भी है।)
टोपीवाला : (पूर्ववत् राह-चलतों को सुनाकर) मसीह की सबसे बड़ी करामात यह थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। उन्होंने जेरस की मुर्दा बेटी को छुआ और वो उठ बैठी तो वो क्यों आकर मेरी इस मुर्दा मछली को नहीं जिलाते। (दरवाजे की ओर देखकर) निकालो अपने उस मसीह को कि मेरी इस मुर्दा मछली को जिंदा करे।
(कुछ और लोग आ जाते हैं, जिनमें एक कृपाणवाला भी है।)
चोटीवाला : (आगे बढ़कर) क्यों भाई क्या बात है ?
टोपीवाला : ‘अल मुबल्लिग’ में मैंने एक मारके का मजमून लिखा था, जिसमें ईसाई मजहब की बुनियादी खामियों पर दलील के साथ बहस की थी। मेरे इस लेख का कोई माकूल1 जवाब देने के बदले (सोसाटी के दरवाजे की ओर देखकर) पादरी बधावा-राम ने अपने अखबार के रसूले-पाक की करामातों पर एतराज किया है। मेराज2 की असलियत को समझना पादरी बधावाराम के बस की बात नहीं। कौन नहीं जानता कि खुदाबन्दे करीम ने अपने रसूल को सातों आसमानों की सैर करायी और वो भी इतने कम अर्से में कि जिस दरवाजे से रसूल-पाक गये थे, उसकी कुण्डी उनके वापस आने पर अभी हिल रही थी। इस मोजजे3 के कई मतलब निकल सकते हैं, लेकिन उन पर गौर करने के बजाय पादरी बधवाराम ने ओछे और लगव4 एतराज किये हैं।
कृपाणवाला : पर मियां, इस टीन के डिब्बे में क्या है ?
टोपीवाला : मछली।
कृपाणवाला : मछली !
टोपीवाला : हां, मुर्दा मछली ! मैं पादरी बधावाराम को चैलेंज देने आया हूं कि अगर सचमूच यीसू मसीह में यह ताकत थी कि वे मुर्दों को जिंदा कर देते थे और अगर सचमुच वो खुदा के बेटे थे, तो पादरी वधावाराम अपने उस खुदा के बेटे को बुलाये कि वो आकर मेरी इस मुर्दा मछली को जिलाये और अपनी मसीहाई का सुबूत दे।
चोटीवाला : पादरी बधावाराम ! (चोटी पर हाथ फेर और हंसते हुए अपने पास खड़े एक-दूसरे लंबी चोटीवाले साथी से) अरे ! यह वही बधावाराम है, जिसे हमने शुद्ध किया था परंतु जो हमारे कठिन सिद्धांत पर पूरा न उतर सका था।
(पादरी बधावाराम सोसायटी के दरवाजे से झांकते हैं।)
: (पादरी की ओर देखकर) हां पादरी साहब, बुलाइये अपने खुदा के बेटे को कि वह अपना चमत्कार दिखाकर इस मरी हुई मछली को पुनः जीवित करे (लोगों को सुनाकर) यदि भगवान अमर और सर्वव्यापक हैं तो भगवान का पुत्र अमर और सर्वव्यापक क्यों न होगा और क्यों न यहां आकर इस मुर्दा मछली को जीवित करेगा।
(कुछ लोग भीड़ में आकर सम्मिलित हो जाते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध चुपचाप भीड़ के एक ओर खड़ा तमाशा देखने लगता है।
एक हाथ में बैग उठाये और दूसरे में घंटी लिए एक व्यक्ति सबसे पीछे आकर खड़ा हो जाता है।)
----------------------------------------------------
1. माकूल-युक्तियुक्त। 2. मेंराज-पराकाष्ठा। 3. मोजजा-चमत्कार। 4. लगव-लचर।
टोपीवाला: (घंटी को देखकर नारा लगाता है।) आये खुदा का बेटा और मेरी इस मुर्दा मछली को जिंदा करे।
(पादरी बधावाराम फिर अंदर चले जाते हैं।)
चोटीवाला : (शिखा पर हाथ फेरते हुए) एक सभा में पादरी बधावाराम ने आर्यसमाजियों को मूस-पंथी कहा था—चूहे को शिवलिंग पर से प्रसाद उड़ाते देखकर महर्षि को जो दैवी प्रेरणा मिली थी, उसका उपहास उड़ाते हुए उनके व्यक्तित्व की निंदा की थी। (भाषण देने के अंदाज में हवा में हाथ घुमाते और एड़ियां उठाते हुए) महर्षि दयानंद पूर्ण ब्रह्मचारी थे, उनके मुख पर अद्भुत, अलौकिक तेज और उनके अंगों में अपार शक्ति थी। अपने योगबल से वे ऐसे आश्चर्यजनक बातें कर सकते थे, जो दूसरों को चमत्कार मालूम होती थीं। जालंधर में टिक्का साहब की गाड़ी को उन्होंने पीछे से पकड़ लिया। घोड़े शक्ति लगाकर थक गये। लेकिन वह तो ब्रह्मचारी का बल था, टस से मस न हुई गाड़ी। चमत्कार यह होता है। इसे बुद्धि स्वीकार करती है, परंतु....
कृपाणवाला : (जोश में आगे बढ़कर) इन्हीं पादरी साहब ने हमारे बाबा साहब बाबा गुरुनानक के चमत्कारों की भी आलोचना की थी और मोदीखाने की बात को लेकर मजाक उड़ाया था। वे तो सत्यावान1 पुरुष थे। ननकाना साहब के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। गुरु साहब के बहनोई जयगोपाल लोधी सुल्तान के यहां नौकर थे।
----------------------------------------------
1. सत्यावान—शक्तिशाली
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book